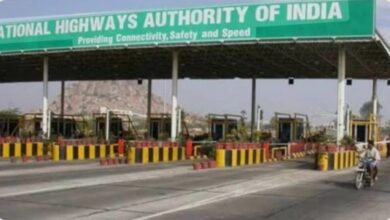आरएसएस के 100 वर्ष : जांच के घेरे में एक सदी
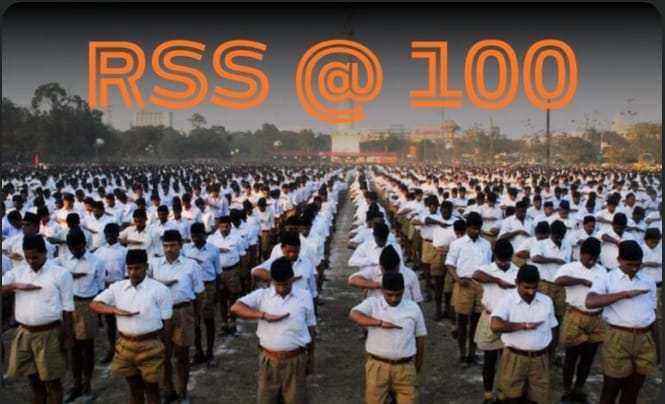
आरएसएस के 100 वर्ष : जांच के घेरे में एक सदी
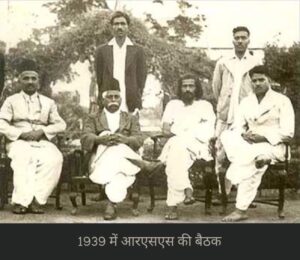
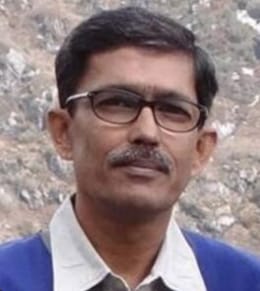
हसनैन नक़वी
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) इस वर्ष अपनी शताब्दी मना रहा है। 27 सितंबर 1925 को नागपुर में डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित, आरएसएस देश के सबसे शक्तिशाली गैर-राजनीतिक संगठनों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। इसके प्रख्यात संगठनात्मक अनुशासन और सामाजिक लामबंदी ने गहरे राजनीतिक प्रभाव को जन्म दिया है। फिर भी, इस शक्ति के साथ-साथ एक जटिल और विवादास्पद विरासत भी जुड़ी हुई है — जिसकी भारत के संवैधानिक आदर्शों, बहुलतावादी संकल्प और सामाजिक न्याय की अनिवार्यताओं के आलोक में जाँच की जानी चाहिए।
धीरेंद्र के. झा, ” शैडो आर्मीज़: फ्रिंज ऑर्गनाइज़ेशन्स एंड फुट सोल्जर्स ऑफ़ हिंदुत्व” (2019) में , आगाह करते हैं कि संघ को केवल एक सांस्कृतिक समाज के रूप में नहीं, बल्कि “घेरे में फंसे एक समुदाय की रक्षा के लिए एक अनुशासित हिंदू मिलिशिया” के रूप में डिज़ाइन किया गया था (झा 2019, पृष्ठ 13)। यह ढाँचा इस बात को समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि कैसे, समय के साथ, आरएसएस के उद्देश्य और कार्य अक्सर बहिष्कार और वैचारिक कठोरता के पैटर्न से टकराते रहे हैं।
आधारभूत दोष रेखाएँ : जाति, लिंग और नेतृत्व बहिष्कार
हालाँकि आरएसएस खुद को हिंदू एकता की ताकत के रूप में पेश करता है, लेकिन अपने शुरुआती वर्षों से ही इसने अपने भीतर गहरे सामाजिक पदानुक्रम को फिर से स्थापित किया है। नीलांजन मुखोपाध्याय, ” आरएसएस: आइकॉन्स ऑफ़ द इंडियन राइट” (2009) में लिखते हैं कि “सामाजिक समरसता के ढिंढोरा पीटने के बावजूद, संघ ऊँची जातियों का ही गढ़ बना रहा, जिसमें नेतृत्व की भूमिकाओं में दलितों (आदिवासियों) या पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व नगण्य था” (मुखोपाध्याय, 2009, पृष्ठ 45)।
यह बहिष्कार लैंगिक गतिशीलता में भी परिलक्षित होता है। महिलाओं को कभी भी आरएसएस में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें अलग से संगठित राष्ट्रीय सेविका समिति में शामिल किया जाता है। शम्सुल इस्लाम ने ” आरएसएस, स्कूली पाठ्यपुस्तकें और महात्मा गांधी की हत्या” (2013) में इस व्यवस्था को प्रतीकात्मक बताया है : “संघ की समाज की कल्पना गहन रूप से पितृसत्तात्मक है, जहाँ महिला को परंपराओं की संरक्षक माना जाता है, न कि नेतृत्व में समान भागीदार” (इस्लाम 2013, पृष्ठ 98)।
वैचारिक असंगति : संवैधानिक सिद्धांतों का प्रतिरोध
आरएसएस के मूलभूत सिद्धांत भारत की संवैधानिक व्यवस्था से टकराते थे। संघ के दूसरे सरसंघचालक गोलवलकर ने धर्मनिरपेक्ष, बहुलतावादी शासन के विचार को अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने “बंच ऑफ़ थॉट्स” (1966) में लिखा, “हमारे संविधान की सबसे बुरी बात यह है कि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे हमारा अपना कहा जा सके।” गोलवलकर ने संविधान की भावना का खुलेआम मज़ाक उड़ाया और उसे विदेशी बताया। उन्होंने लिखा कि अल्पसंख्यकों को “केवल सह-अस्तित्व में रहना चाहिए, आत्मसात नहीं किया जाना चाहिए” और चेतावनी दी कि हिंदू संस्कृति और विश्वदृष्टि को अपनाने से इंकार करने से वे राष्ट्रीय एकता के लिए “खतरा” बन जाते हैं (बंच ऑफ़ थॉट्स, पृष्ठ 52)।
यह तिरस्कार सामाजिक समानता तक भी फैला हुआ था। गोलवलकर के लिए, जातिगत पदानुक्रम “स्वाभाविक” था और सामाजिक व्यवस्था का अभिन्न अंग था। उन्होंने समतावाद को पश्चिमी संदूषण बताते हुए खारिज करते हुए तर्क दिया, “जातिविहीन समाज का विचार काल्पनिक है।”
एक शांत दर्शक : आरएसएस और स्वतंत्रता संग्राम
भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण दौर —उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष — में आरएसएस अलग-थलग खड़ा रहा। व्यापक राजनीतिक लामबंदी के बजाय, इसने आंतरिक रूप से ध्यान केंद्रित किया और सांस्कृतिक शक्ति का विकास किया। विद्वानों ने बताया है कि संघ ने भारत छोड़ो आंदोलन और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अन्य महत्वपूर्ण अभियानों से काफ़ी हद तक दूरी बनाए रखी। गांधी, नेहरू, बोस और आज़ाद जैसे नेताओं के जेल जाने के बावजूद, आरएसएस ने चुप्पी साधे रखी।
बीआर अंबेडकर ने प्रसिद्ध रूप से टिप्पणी की थी कि संघ संघर्ष के दौरान “अलग-थलग” रहा (अंबेडकर, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, 1945)। यहाँ तक कि सरदार वल्लभभाई पटेल ने भी राष्ट्रीय हित में इसके सीमित योगदान के लिए आरएसएस की आलोचना की थी।
हिंसा की छाया : गांधी की हत्या और उसके बाद की स्थिति
जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या आधुनिक भारत के सबसे काले अध्यायों में से एक है। गांधीजी के हत्यारे नाथूराम गोडसे का संबंध आरएसएस से था। हालाँकि संघ ने औपचारिक रूप से इसमें शामिल होने से इंकार किया, लेकिन सरकार ने उस पर लगभग दो साल का प्रतिबंध लगा दिया।
सरदार पटेल ने सितंबर 1948 में एमएस गोलवलकर को लिखा था कि “उनके [आरएसएस के] सभी भाषण सांप्रदायिक जहर से भरे थे… उन्होंने देश में ऐसा माहौल बनाया, जिसमें इतनी भयावह त्रासदी संभव हो सकी” (पटेल, कलेक्टेड वर्क्स, खंड 10, पृष्ठ 395)।
गोपनीयता, प्रतिबंध और जवाबदेही की कमी
अपने 100 वर्षों के इतिहास में, आरएसएस ने कई प्रतिबंधों का सामना किया है – 1948 (गांधीजी की मृत्यु के बाद), 1975 (आपातकाल के दौरान), और फिर 1992 (बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद)। फिर भी, हर बार, यह और मज़बूत होकर उभरा और शिक्षा, मीडिया, ट्रेड यूनियनों और नागरिक समाज में अपनी पहुँच का विस्तार किया। हालाँकि, यह वृद्धि सीमित पारदर्शिता के साथ हुई है। अपने व्यापक प्रभाव के बावजूद, आरएसएस को एक राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि एक “सांस्कृतिक संगठन” के रूप में पंजीकृत किया गया है, जो इसे सार्वजनिक जाँच और लोकतांत्रिक जवाबदेही से बचाता है।
हाशिये से मुख्यधारा तक : राजनीतिक सहजीवन
आरएसएस और उसकी राजनीतिक शाखा, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने एक राष्ट्रवादी आख्यान को सिद्ध कर दिया है, जिसने सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया है। संघ, भाजपा के पीछे एक प्रमुख वैचारिक, कैडर-भर्ती और नीति-निर्माण शक्ति, के रूप में कार्य करता है। जैसा कि क्रिस्टोफ़ जैफ्रेलॉट कहते हैं, “हिंदू राष्ट्र अब एक अमूर्त स्वप्न नहीं रहा ; इसे कानून बनाया जा रहा है, सामान्य बनाया जा रहा है और संस्थागत रूप दिया जा रहा है” (हिंदू राष्ट्रवाद, 2021, पृष्ठ 101)।
सत्तावादी प्रतिध्वनियाँ : विदेशी प्रभाव और वैचारिक समानताएँ
गोलवलकर ने यूरोपीय फ़ासीवादी मॉडलों से प्रेरणा ली। “वी, ऑर अवर नेशनहुड डिफाइंड” (1939) में, उन्होंने नाज़ी जर्मनी की उसके “नस्लीय गौरव” और अल्पसंख्यकों के “शुद्धिकरण” के लिए प्रशंसा की। विद्वानों ने इन प्रतिध्वनियों को आकस्मिक से अधिक बताया है, जो बहुलवाद, असहमति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति शत्रुतापूर्ण विश्वदृष्टि का संकेत देते हैं, (फ़ासीवाद और राष्ट्रवाद, 2019, पृष्ठ 48-53)।
एक स्पष्ट गणना की ओर
आरएसएस के सौ साल पूरे होने के साथ, इसकी विरासत कड़ी समीक्षा की मांग कर रही है। इसके मूल बहिष्कारवादी रुझान, संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिरोध और लोकतंत्र के प्रति द्वैधता भारत के बहुलतावादी दृष्टिकोण के साथ असहज रूप से मेल नहीं खाते। मूल प्रश्न यह है कि क्या एक सौ साल पुराना संगठन, जो कभी स्वतंत्रता संग्राम से अलग खड़ा था और संवैधानिक आदर्शों के प्रति तिरस्कार का भाव रखता था, गणतंत्र की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के साथ सार्थक रूप से जुड़ सकता है?(हसनैन नक़वी इतिहासकार और सेंट जेवियर्स कॉलेज, मुंबई के इतिहास संकाय के सदस्य हैं। यह लेख मूलतः दिल्ली से प्रकाशित “द इमर्जिंग वर्ल्ड” दैनिक में प्रकाशित हुआ था।)